जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो चार वेद, अठारह पुराण, 108 उपनिषद और छह शास्त्रों का जिक्र जरूर होता है। चार वेदों और अठारह पुराणों के नाम तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन छह शास्त्रों के बारे में सभी को पूरी जानकारी नहीं होती। इन छह शास्त्रों को ही “षड् दर्शन” कहा जाता है।
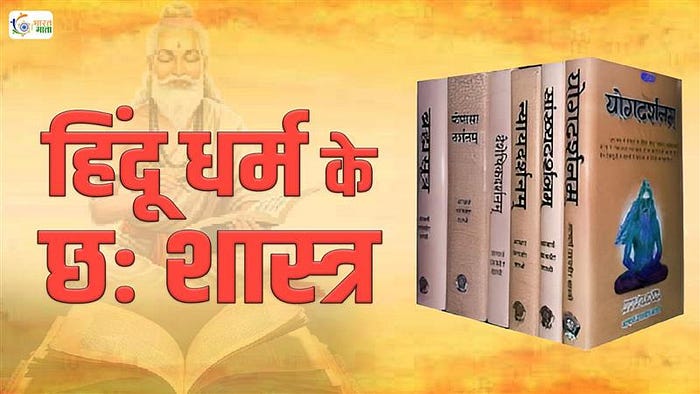
“शास्त्र” संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है उपदेश, नियम या अनुशासन। ये विशेष विषय पर लिखे गए ग्रंथ होते हैं। महान ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन करके इन छह शास्त्रों की रचना की है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा है और इसकी जड़ें चार वेदों में हैं। इन्हीं वेदों को आधार बनाकर कई ऋषियों ने दर्शन की गहरी नींव तैयार की और अध्यात्म के रहस्यों को समझाने के लिए ये छह शास्त्र लिखे।
हिंदू धर्म के 6 शास्त्र और उनके रचयिता
- महर्षि गौतम रचित — न्याय शास्त्र
- महर्षि पतंजलि रचित — योग शास्त्र
- महर्षि कपिल रचित — सांख्य शास्त्र
- महर्षि कणाद रचित — वैशेषिक शास्त्र
- महर्षि वेदव्यास रचित — वेदांत शास्त्र
- महर्षि जैमिनि रचित — मीमांसा शास्त्र
आइए अब हम इन सभी शास्त्रों को विस्तार से समझते हैं।
1. न्याय शास्त्र — तर्क और न्याय का विज्ञान
न्याय शास्त्र की रचना महर्षि गौतम ने की थी। इस शास्त्र में बताया गया है कि पदार्थों के सच्चे ज्ञान से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार जब हमें ब्रह्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो हम झूठ से, बुरे कर्मों से, दुखों से और मोह से मुक्त हो जाते हैं। इस शास्त्र में ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान माना गया है। यह भी बताया गया है कि शरीर और आत्मा अलग-अलग हैं।
न्याय शास्त्र में एक प्रसिद्ध सूत्र है — “प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्यायः” — यानी प्रमाणों के द्वारा किसी बात की सही परीक्षा करना ही न्याय है। इसलिए इस शास्त्र को तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस शास्त्र को तीन भागों में बांटा गया है — आदिकाल, मध्यकाल और अंत्यकाल।
न्याय शास्त्र में कुल 16 विषय बताए गए हैं जिनमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान शामिल हैं। इन सोलह पदार्थों के सच्चे ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शास्त्र में न्याय करने की सही विधि के साथ-साथ जीत और हार के कारणों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।
2. योग शास्त्र — साधना और समाधि का मार्ग
महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा का संपूर्ण वर्णन मिलता है। योग शास्त्र में योग, चित्त, प्राण, आत्मा की वृत्तियां, इनको नियंत्रित करने के उपाय, जीव के बंधन का कारण जैसी यौगिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। यौगिक क्रिया के माध्यम से परमात्मा का ध्यान आंतरिक हो जाता है। जब तक हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों में लगी रहती हैं, तब तक ध्यान लगाना असंभव होता है।
महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। योग शास्त्र में भी पच्चीस तत्व हैं जो सांख्य शास्त्र में दिए गए हैं। योग शास्त्र चार भागों में बंटा है — समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। समाधि भाग में योग का अर्थ और लक्ष्य बताया गया है। साधन भाग में कर्मफल और क्लेश का वर्णन है। विभूति भाग में योग के अंग और उनके परिणाम बताए गए हैं तथा अणिमा, महिमा जैसी सिद्धियां कैसे प्राप्त करें यह समझाया गया है। कैवल्य भाग में मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं।
योग शास्त्र का सार यह है कि प्रकृति के चौबीस भेद और आत्मा तथा ईश्वर — इस तरह कुल छब्बीस तत्व हैं। प्रकृति जड़ है और निरंतर बदलती रहती है, जबकि मुक्त पुरुष और ईश्वर नित्य, चेतन, स्वप्रकाश, आसक्ति रहित, देश-काल से परे और पूर्णतया निर्विकार हैं।
3. सांख्य शास्त्र — पुरुष और प्रकृति का दर्शन
महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र का मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद के अनुसार सृष्टि का मूल कारण प्रकृति है। सांख्य शास्त्र का स्पष्ट मत है कि अभाव से भाव या असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। यानी किसी वास्तविक कारण से ही सच्चे कार्य की उत्पत्ति होती है।
सांख्य शास्त्र में प्रकृति से इस सृष्टि की रचना और संहार के क्रम का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें पुरुष को चेतन तत्व और प्रकृति को अचेतन तत्व माना गया है। पुरुष प्रकृति का भोग करने वाला है, परंतु प्रकृति स्वयं का भोग नहीं करती।
सांख्य शास्त्र भारत का बहुत प्राचीन और आस्तिक शास्त्र है। “सांख्य” शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान तथा संख्या बताया गया है। सांख्य शास्त्र के ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत महर्षि कपिल का ‘सांख्य सूत्र’ और ईश्वरकृष्ण रचित ‘सांख्य कारिका’ है। इस शास्त्र में विकासवाद का समर्थन किया गया है और बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति के सहयोग से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है।
4. वैशेषिक शास्त्र — पदार्थों का विज्ञान
महर्षि कणाद ने वैशेषिक शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में धर्म को सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। वैशेषिक शास्त्र के अनुसार लौकिक प्रशंसा और परम कल्याण के साधन को धर्म कहा गया है। इसलिए मानव कल्याण के लिए धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है।
वैशेषिक शास्त्र में सात पदार्थ बताए गए हैं — द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य नौ प्रकार के हैं — पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, काल, दिशा, आत्मा और मन। वैशेषिक मत के अनुसार जड़ पदार्थों के तत्व ज्ञान के बिना आत्मतत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मुक्ति के लिए आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस शास्त्र में जड़ पदार्थों की भी विस्तार से व्याख्या की गई है।
5. वेदांत शास्त्र — ब्रह्म ज्ञान का सार
महर्षि वेदव्यास ने वेदांत शास्त्र की रचना की है। “वेदांत” का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत या वेदों का सार। वेदव्यास रचित ‘ब्रह्मसूत्र’ को वेदांत शास्त्र का मूल ग्रंथ माना जाता है। वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ही सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है।
वेदांत शास्त्र में कहा गया है “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” — यानी जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, वह ब्रह्म से अलग है, नहीं तो स्वयं को जानने की इच्छा कैसे होती? सब कुछ जानने वाला जीवात्मा हमेशा अपने दुखों से मुक्त होने के उपाय खोजता रहता है। परंतु ब्रह्म का गुण जीवात्मा से भिन्न है।
वेदांत शास्त्र ज्ञानयोग का स्रोत है जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को भी ‘वेदांत’ कहा जाता है। उपनिषद को वेदों, ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार माना जाता है।
वेदांत की तीन प्रमुख शाखाएं हैं — अद्वैत वेदांत (आदि शंकराचार्य द्वारा), विशिष्टाद्वैत (रामानुजाचार्य द्वारा) और द्वैत वेदांत (माधवाचार्य द्वारा)। अद्वैत में ब्रह्म और आत्मा को एक माना जाता है, विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म, जीव और जगत को सत्य माना जाता है, जबकि द्वैत में तीनों को पूरी तरह अलग-अलग माना जाता है।
6. मीमांसा शास्त्र — कर्मकांड का विज्ञान
महर्षि जैमिनि ने मीमांसा शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में वैदिक यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्रों का विभाजन और यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार यज्ञों के मंत्र, श्रुति, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या को मूल आधार माना जाता है।
इस शास्त्र में राष्ट्र की उन्नति के लिए मनुष्य के पारिवारिक जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन के कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए। महर्षि जैमिनि ने धर्म के लिए वेद को ही मुख्य प्रमाण माना है।
मीमांसा को दो भागों में बांटा जाता है — पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वेदों के कर्मकांड (कर्म काण्ड) से संबंधित विषय हैं, जबकि उत्तर मीमांसा में वेदों के ज्ञानकाण्ड से संबंधित विषय हैं, जिसे वेदांत भी कहा जाता है।
छह शास्त्रों में समानताएं
भले ही ये छह शास्त्र अलग-अलग विषयों पर हैं, लेकिन इन सभी में कुछ समानताएं हैं:
1. मंगलाचरण: सभी शास्त्रों की शुरुआत वैदिक मंगलाचरण ‘अथ’ शब्द से होती है।
2. विषय प्रस्तुति: हर शास्त्र के पहले सूत्र में ही उसका मुख्य विषय बता दिया जाता है।
3. व्याख्या शैली: सभी शास्त्र अपने उद्देश्य को बताते हैं, फिर उसकी परिभाषा देते हैं और फिर गहराई से उसकी परीक्षा करते हैं।
4. संक्षिप्त भाषा: सभी शास्त्रों की भाषा शैली संक्षिप्त और सटीक है।
5. विस्तृत ज्ञान: शास्त्र अपने मुख्य विषय के साथ-साथ उपविषयों का भी ज्ञान देते हैं।
6. वेद प्रमाण: सभी शास्त्र वेदों को अपना प्रमाण स्वीकार करते हैं।
7. पूरकता: ये शास्त्र एक-दूसरे की कमी को पूरा करने वाले हैं। एक शास्त्र में जो बात छूट जाती है, दूसरा उसे पूरा कर देता है।
षड् दर्शन का महत्व
ये छह शास्त्र या षड् दर्शन हिंदू धर्म की दार्शनिक नींव हैं। इन्हें समझने से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ मिलती है:
न्याय शास्त्र हमें तर्क करना और सही-गलत की पहचान करना सिखाता है। योग शास्त्र हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। सांख्य शास्त्र हमें आत्मा और प्रकृति के रहस्य बताता है। वैशेषिक शास्त्र हमें भौतिक जगत की समझ देता है। वेदांत शास्त्र हमें परम सत्य का ज्ञान कराता है। मीमांसा शास्त्र हमें कर्तव्य और धर्म का पाठ पढ़ाता है।
इन सभी शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य एक ही है — मनुष्य को दुख से मुक्त करना और मोक्ष की ओर ले जाना। ये केवल पुराने ग्रंथ नहीं हैं बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं।
आधुनिक समय में प्रासंगिकता
आज के युग में भी इन शास्त्रों की बहुत प्रासंगिकता है। योग आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और लाखों लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। न्याय शास्त्र के तर्क और प्रमाण के सिद्धांत आज भी कानून और न्याय व्यवस्था में उपयोगी हैं। वेदांत दर्शन ने स्वामी विवेकानंद के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। सांख्य दर्शन की अवधारणाएं आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाती हैं।
इन शास्त्रों को पढ़ना और समझना केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व विकास, मानसिक शांति और जीवन की गहरी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और उपयोगी है।
निष्कर्ष
हिंदू धर्म के ये छह शास्त्र या षड् दर्शन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्होंने न केवल भारतीय दर्शन को समृद्ध किया है बल्कि पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित किया है। ये शास्त्र हमें बताते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख-दुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य है।
इन शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें जीवन के हर पहलू — चाहे वह तर्क हो, कर्म हो, ध्यान हो या आत्मज्ञान — की समझ मिलती है। आज के तनावपूर्ण जीवन में इन प्राचीन शास्त्रों की शिक्षाएं हमें शांति, संतुलन और सही दिशा दे सकती हैं।
Comments
Post a Comment